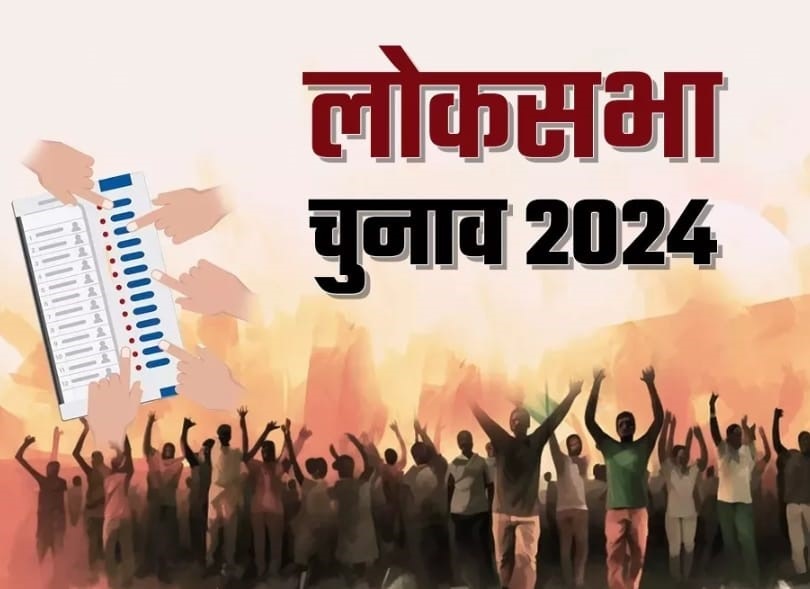बंधनों को खोलने का ‘सेफ्टी वॉल्व’ है होली
हेमंत शर्मा
होली, बनारस, शिव, मस्ती, भांग और ठण्डाई इन्हें अलगाया नहीं जा सकता। यह उतना ही सच है जितना ‘ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या।’ बनारस की होली के आगे सब मिथ्या लगता है। आज भी लगता है कि असली होली उन शहरों में हुआ करती थी, जिन्हें हम पीछे छोड़ आए हैं। ऐसी होली जहां सब एक साथ इकट्ठे होते, खुशियों के रंग बंटते, जहॉं बाबा भी देवर लगते और होली का हुरियाया साहित्य बॉंचा जाता। जिसमें समाज राजनीति और रिश्ते पर तीखी चोट होती। मुझे जीवन के यही संस्कार बनारस से मिले हैं। शहर बदला, समय बदला मगर संस्कार कहां बदलते हैं? मैं नोएडा में भी एक बनारस इक्कठा करने की कोशिशों में लगा रहता हूं। इस बार की रंगभरी एकादशी पर ऐसा ही हुआ। दोस्त, यार इकट्ठा हुए। उत्सव, मेलजोल, आनंद के लिए। खिलाना पिलाना तो होता ही है। मगर सबसे अहम था जीवन की इस आपाधापी के बीच कुछ देर के लिए ही सही, साथ-साथ होना और साथ-साथ जीना। ऋग्वेद भी कहता है “संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनासि जानताम।” अर्थात हम सब एक साथ चलें। आपस मे संवाद करें। एक दूसरे के मनो को जानते चलें।
फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, रंगभरी एकादशी होती है। कथा है कि शिवरात्रि पर विवाह के बाद भगवान शिव ससुराल में ही रह गए थे। रंगभरी को उनका गौना होता है। गौरी के साथ वे अपने घर लौटते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होली खेल कर करते हैं। इसीलिए काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी से ही बाबा का होली कार्यक्रम शुरू होता है। उस रोज़ मंदिर में होली होती है। दूसरे रोज़ महाश्मशान में चिता भस्म के साथ होली खेली जाती है। शिव यहीं विराजते हैं। सो उत्सव के लिए इससे अधिक समीचीन दूसरा मौका कहां होगा! वैसे भी होली समाज की जड़ता और ठहराव को तोड़ने का त्योहार है। उदास मनुष्य को गतिमान करने के लिए राग और रंग जरूरी है। होली में दोनों हैं। यह सामूहिक उल्लास का त्योहार है। परंपरागत और समृद्ध समाज ही होली खेल और खिला सकता है। रूखे और बनावटी आभिजात्य को ओढ़ने वाले समाज का यह उत्सव नहीं है। सांस्कृतिक लिहाज से दरिद्र व्यक्ति होली नहीं खेल सकता। वह इस आनंद का भागी नहीं बन सकता। साल भर के बंधनों, कुंठा और भीतर जमी भावनाओं को खोलने का ‘सेफ्टी वॉल्व’ है होली।
मैं होली के बहाने मित्रों को इक्कठा करता हूँ। बनारस में था तो घर में रंगभरी होती थी। लखनऊ आया तो वहॉं भी हर बरस रंगभरी का सिलसिला टूटा नहीं। लखनऊ में भी खानपान और संगीत बनारस का ही होता था। पं छन्नूलाल मिश्र सहित कई गायक इस जमावड़े में गा चुके हैं। जब दिल्ली आया तो यहॉ उस आत्मीयता की जड़ें ही सूखी थीं जो बनारस या लखनऊ में मिलती थीं। मेरे लिए ये एक सांस्कृतिक झटका सा था। मगर मेरा आयोजन जारी रहा। एकाध बार व्यस्तता और पिछले साल कोरोना के कारण सिलसिला टूटा। रंगभरी के आयोजन का समय बदला, पर स्वाद नहीं। सुप्रियो प्रसाद मुझे इस पार्टी की पूरे साल याद दिलाते रहते हैं। यह रंगभरी इस लिहाज से खास थी कि कोरोना के एक साल बाद कोई ऐसा जमावड़ा था। जहॉं विचार और व्यवहार से अलग-अलग पत्रकारीय साथी एक साथ थे। बनारस के दिनों के मेरे साथी। लखनऊ की पत्रकारिता के मित्र गण। दिल्ली-नोएडा के संगी-साथी। सब जमा थे। पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी तक की प्रिंट और टीवी पत्रकारिता का पूरा विमर्श इस सांस्कृतिक उत्सव में मौजूद था। हमारी संस्कृति में उत्सव कलाओं को शोकेस करते हैं। सो होरी भी गाई गई और लोकगीतों के मोती भी बिखरे। महाकवि कुमार विश्वास, पद्मश्री मालिनी अवस्थी, और गायक सॉंसद मनोज तिवारी ‘मृदुल’ ने मिलकर उत्सव के इस लोक को जीवन में उतार दिया। रंगभरी एकादशी के मूल में उत्सव की परंपरा है, सो आयोजन के हर पहलू को परंपराओं से लबालब होना चाहिए। इसीलिए खानपान भी होली की परम्परा के थे। फिर भी कोशिश रही कि एक दिन के लिए सही, बनारस के जायके को दिल्ली की जुबान पर लाया जाए। सो पार्टी में बनारस के दीना की मशहूर चाट से लेकर पाठक जी की पंचरतनी तक सब मौजूद था। ठण्डाई को ही पंचरतनी कहते हैं क्योंकि इसमें पॉंच भयंकर चीजें मिलाई जाती है। इसमें भॉंग, काली मिर्च, तूतिया, धतूरा, शंखिया जैसे पॉच प्रचण्ड अवयव होते है। पारम्परिक ठण्डाई में पॉंच वेजेटेबिल लौकी, खीरा, खरबूज, तरबूज़ और कोहडे़ के बीज भी होते हैं। इन पंचरतनां के साथ ठंडाई का मूल आनंद मिले, इसलिए मैंने बनारस से ठंडाई वालों को बुलाया था। सैकड़ों बरस से जिनका यह पुश्तैनी काम है। बनारसी ठसक कायम रखने के लिए ये ठंडाई वाले कोल्डचेन में सुरक्षित कर दूध और मलाई भी बनारस से ही लाए थे। ठंडाई और भांग का एक अद्भुत आपसी मेल है। भॉंग की तासीर को ठंडा करने के लिए ठंडाई का आविर्भाव हुआ। इसकी भी एक कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से निकला विष भगवान शिव ने पीकर अपने गले में धारण कर लिया था। हलाहल विष से उन्हें बहुत गर्मी लगने लगी। शरीर नीला पड़ना शुरू हो गया। फिर भी शिव पूर्णतः शांत थे। तब देवताओं और वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने भगवान शिव की तपन को शांत करने के लिए उन्हें जल चढ़ाया और विष का प्रभाव कम करने के लिए विजया (भांग का पौधा), बेलपत्र और धतूरे को दूध में मिलाकर (ठंडाई) भगवान शिव को औषधि रूप में पिलाया। इससे वे विष की गर्मी भी झेल गए थे। तभी से ठंडाई में भांग मिलाकर शिव को भोग लगाते है।
रंगभरी के प्रचण्ड आयोजन में विजया, पंचरतनी, मुनक्का, षडरस, रसरंजन का चौचक इंतज़ाम था। लोगों इस स्वाद का झूम कर आनन्द भी लिया। हमारी परम्परा में चाट षड रसों का घनीभूत स्वाद है। षड-रस में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय समेत समस्त प्रकार के रस विद्यमान थे। कोई भी भोजन हो, इन छहों रसों की उपस्थिति होनी चाहिए। चाट के साथ ‘रसरंजन’ का भी इंतजाम था। कॉकटेल के लिए रसरंजन नाम नामवर जी के परामर्श से स्वर्गीय डीपी त्रिपाठी ने गढ़ा था। ’रसरंजन’ हिन्दी साहित्य में डीपी त्रिपाठी का अवदान है। वे इस आयोजन के स्थायी भाव होते थे। उनकी बहुत याद आई। खानपान की इस परंपरा का एक सनातन विमर्श भी है। शिव को भंग पसंद है। वे हमेशा उसकी तरंग में रहते है। इसलिए बिना भंग कैसी रंगभरी। तभी तो भारतीय वॉंग्मय में भॉंग का दूसरा नाम शिव प्रिया और विजया भी है। शिवजी को प्रिय भांग औषधीय गुणों से भरी पड़ी है। अंग्रेज़ी में इसे कैनाबीस, बीड कहते है। जिसमें टेट्रा हाइड्रोकार्बन बिनोल पाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मैंगनीज, विटामिन ई, मैग्नीशिम एवं फास्फोरस समेत कई पोषक तत्व होते हैं। इसे सही मात्रा में लेने से कोलेस्ट्राल नियंत्रित रहता है। क्योंकि भॉंग खून को प्यूरिफाई करने का काम करता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में इसका ज़िक्र है। सुश्रुत संहिता में गांजे के चिकित्सीय प्रयोग की जानकारी मिलती है। सुस्ती, नजला और डायरिया में इसके इस्तेमाल का उल्लेख है। अथर्ववेद में जिन पांच पेड़-पौधों को सबसे पवित्र माना गया है उनमें भांग का पौधा भी शामिल है। इसे मुक्ति, खुशी और करुणा का स्रोत माना जाता है। इसके मुताबिक भांग की पत्तियों में देवता निवास करते हैं। अथर्ववेद इसे ‘प्रसन्नता देने वाले’ और ‘मुक्तिकारी’ वनस्पति का दर्जा देता है : पञ्च राज्यानि वीरुधां सोमश्रेष्ठानि ब्रूमः। दर्भो भङ्गो यवः सह ते नो मुञ्चन्त्व् अंहसः।। पांच पौधों में सोम श्रेष्ठ है। ऐसी औषधियों के पांच राज्य, दर्भ, (भङ्ग) भांग, (यवः) जौ और (महः) बलशाली धानको (ब्रूमः) हम कहते हैं कि वे हम सबको पापसे बचावें। कहते हैं भांग और धतूरे के सेवन से ही भगवान शिव हलाहल विष के प्रभाव से मुक्त हुए थै। इसलिए शंकर को भंग पंसद है।
होली, ठंडाई, और बनारस .. ये महज तीन शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला हैं। इसमें कला भी है, साहित्य भी, विज्ञान और अध्यात्म भी। यहां बरसों से आबाद ठंडाई की दुकानें सत्ता-साहित्य से जुड़े लोगों का अड्डा रही हैं। जयशंकर प्रसाद और रूद्र जी तो बिना भंग की तंरग के सृजन के आयाम ही नहीं खोलते थे। बनारस का मुनक्का प्रसिद्ध है। मुनक्का का सेवन स्वास्थ्यवर्धक होता है। मुनक्के में काजू किसमिस पिस्ता बादाम का पेस्ट और उसी अनुपात में भॉंग होती है। बहुत ही स्वादिष्ट। मुनक्का संपादक जी को बहुत पंसद है। कई गटक गए। एक डिब्बा साथ भी ले गए। इसका एफ्रोडेसिक एफेक्ट भी होता है। शायद उन्हें मालूम है। भॉंग का भाषा की शुद्धता से भी कोई रिश्ता है क्योंकि हिन्दी का पहला व्याकरण लिखने वाले कामता प्रसाद गुरू, संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद, कथाकार रूद्र काशिकेय, महाप्राण निराला और राहुल देव जी सभी को भांग पसंद है। होली प्रेम की वह रसधारा है, जिसमें समाज भीगता है। ऐसा उत्सव है, जो हमारे भीतर के कलुष को धोता है। होली में राग, रंग, हँसी, ठिठोली, लय, चुहल, आनंद और मस्ती है। इस त्योहार से सामाजिक विषमताएँ टूटती हैं, वर्जनाओं से मुक्ति का अहसास होता है, जहाँ न कोई बड़ा है, न छोटा; न स्त्री न पुरुष; न बैरी, न शत्रु। इस पर्व में व्यक्ति और समाज राग और द्वेष भुलाकर एकाकार होते हैं। किसी एक देवता पर केंद्रित न होकर इस पर्व में सामूहिक रूप से समाज के भीतर देवत्व के गुणों की पहचान होती है। इसीलिए हमारे पुरखों ने होली जैसा त्योहार विकसित किया। हमारे परम्परा में पर्वों के महत्त्व को समझने का मतलब ऋतु परिवर्तन के महत्त्व को समझना है। बसंत के स्वभाव और प्रकृति के हिसाब से उसका असली त्योहार होली ही है। बसंत प्रकृति की होली है और होली समाज की। होली समाज की उदासी दूर करती है। होली पुराने साल की विदाई और नए साल के आने का भी उत्सव है। यह मलिनताओं के दहन का दिन है। अपनी झूठी शान, अहंकार और श्रेष्ठता बोध को समाज के सामने प्रवाहित करने का मौका है। तमस को जलाने का अनुष्ठान है। वैमनस्य को खाक करने का अवसर है।
होली में हमें बनारस का अपना मुहल्ला याद आता है। महानगरों से बाहर निकले तो गाँव, कस्बों और मुहल्ले में ही फाग का राग गहरा होता था। मेरे बचपन में मोहल्ले के साथी घर-घर जा गोइंठी (उपले) माँगते थे। जहाँ माँगने पर न मिलती तो उसके घर के बाहर गाली गाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता। मोहल्ले में इक्का-दुक्का घर ऐसे जरूर होते थे, जिन्हें खूब गालियाँ पड़तीं। जिस मोहल्ले की होलिका की लपट जितनी ऊँची उठती, उतनी ही उसकी प्रतिष्ठा होती। फिर दूसरे रोज गहरी छनती। होलिका की राख उड़ाई जाती। टोलियों में बँटे हम, सबके घर जाते, सिर्फ उन्हें ही छोड़ा जाता जिनके घर कोई गमी होती। मेरे पड़ोसी ज्यादातर यादव और मुसलमान थे, पर होली के होलियारे में संप्रदाय कभी आड़े नहीं आता था। सब साथ-साथ इस हुड़दंग में शामिल होते। अनवर भाई भी वैसे ही फाग खेलते जैसे पं. गिरधर गोपाल। जाति, वर्ग और संप्रदाय का गर्व इस मौके पर खर्च हो जाता।
साहित्य और संगीत होली वर्णन से पटे पड़े हैं। हमारे उत्सवों-त्योहारों में होली ही एकमात्र ऐसा पर्व है, जिस पर साहित्य में सर्वाधिक लिखा गया है। पौराणिक आख्यान हो या आदिकाल से लेकर आधुनिक साहित्य, हर तरफ कृष्ण की ‘ब्रज होरी’ रघुवीरा की ‘अवध होरी’ और शिव की ‘मसान होली’ का जिक्र है। राग और रंग होली के दो प्रमुख अंग हैं। सात रंगों के अलावा, सात सुरों की झनकार इसके हुलास को बढ़ाती है। गीत, फाग, होरी, धमार, रसिया, कबीर, जोगिरा, ध्रुपद, छोटे-बड़े खयालवाली ठुमरी, होली को रसमय बनाती है। उधर नजीर से लेकर नए दौर के शायरों तक की शायरी में होली के रंग मिल जाते हैं। नजीर अकबराबादी होली से अभिभूत हैंकृ‘जब फागुन रंग झमकते हों, तब देख बहारें होली की जब डफ के शोर खड़कते हों, तब देख बहारें होली की।’ तो नए दौर के शायर आलोक श्रीवास्तव ने होली के रंगों को जिंदगी के आईने से देखा है : ‘सब रंग यहीं खेले सीखे, सब रंग यहीं देखे जी के, खुशरंग तबीयत के आगे सब रंग जमाने के फीके।’
वैदिक काल में इस पर्व को नवान्नेष्टि कहा गया, जिसमें अधपके अन्न का हवन कर प्रसाद बाँटने का विधान है। मनु का जन्म भी इसी रोज हुआ था। अकबर और जोधाबाई तथा शाहजहाँ और नूरजहाँ के बीच भी होली खेलने का वृत्तांत मिलता है। यह सिलसिला अवध के नबावों तक चला। वाजिद अली शाह टेसू के रंगों से भरी पिचकारी से होली खेला करते थे। लोक में होली सामान्यतः देवर-भाभी का पर्व है, पर मथुरा के जाव इलाके में राधा-बलराम, यानी जेठ-बहू का हुरंगा भी होता है। पारंपरिक लिहाज से होली दो दिन की होती है। पहले रोज होलिका दहन और दूसरे दिन को धुरड्डी, धुरखेल, धूलिवंदन कहा जाता है। दूसरे रोज रँगने, गाने-बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। देश के कई हिस्सों में पूरे हफ्ते होली मनाई जाती है। ब्रज के अलग-अलग इलाकों बरसाने, नंदगाँव, गोकुल, गोवर्धन, वृदांवन में भी होली का रंग अलग-अलग होता है। लेकिन हर कहीं आनंद, सांस्कृतिक संपन्नता और फसलों का स्वागत इसके मूल में है। बौद्ध साहित्य के मुताबिक, एक दफा श्रावस्ती में होली का ऐसा हुड़दंग था कि गौतम बुद्ध सात रोज तक शहर में न जा बाहर ही बैठे रहे। परंपरागत होली टेसू के उबले पानी से होती थी। सुगंध से भरे लाल और पीले रंग बनते थे। अब इसकी जगह गोबर और कीचड़ ने ले ली है। हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए? सिर चकराने वाले कैमिकल से बने गुलाल, चमड़ी जलाने वाले रंग, आँख फोड़ने वाले पेंट, इनसे बनी है आज की होली।
साहित्य में होली हर काल में रही है। सूरदास, रहीम, रसखान, मीरा, कबीर, बिहारी हर कहीं होली है। होली का एक और साहित्य है हास्य व्यंग्य का। बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ की साहित्य परंपरा इससे अछूती नहीं है। इन हास्य गोष्ठियों की जगह अब गाली-गलौज वाले सम्मेलनों ने ले ली है। जहाँ सत्ता प्रतिष्ठान पर तीखी टिप्पणी होती है। हालाँकि ये सम्मेलन अश्लीलता की सीमा लाँघते हैं, लेकिन चोट कुरीतियों पर करते हैं। होली सिर्फ उऋंखलता का उत्सव नहीं है। वह व्यक्ति और समाज को साधने की भी शिक्षा देती है। यह सामाजिक विषमताओं को दूर करने का त्योहार है। बच्चन कहते हैं ‘भाव, विचार, तरंग अलग है, ढाल अलग है, ढंग अलग, आजादी है, जिसको चाहो आज उसे वर लो। होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो।’ फागुन में बूढ़े बाबा भी देवर लगते थे। वक्त बदला है! आज देवर भी बिना उम्र के बूढ़ा हो शराफत का उपदेश देता है। अब न भीतर रंग है न बाहर। होली मेरे बालकों का कौतुक है या मयखाने का खुमार। कहाँ गया वह हुलास, वह आनंद और वह जोगिरा सा रा रा रा! कहाँ बिला गई है फागुन की मस्ती! इसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। रंगभरी एकादशी के इस उत्सव के बहाने एक बार फिर से इसी बिछड़ी हुई विरासत से मुलाकात हुई। प्रेम बढ़ा। अपनापा गहराया। परंपराएं मिलीं। संस्कार खिले। स्मृतियों के गलियारे से फिर बसंत उतरा। इसी उम्मीद के साथ फिर अगले साल। आप सबको होली की फाल्गुनी शुभकामनाएं।